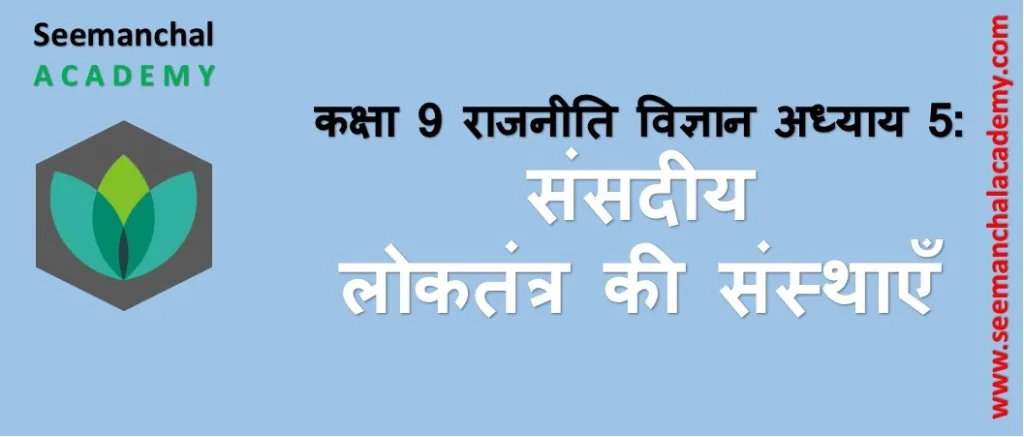
Bihar Board Class 9 राजनीति विज्ञान अध्याय 5 संसदीय लोकतंत्र की संस्थाएँ में लोकतांत्रिक शासन के ढांचे को स्पष्ट करता है।
इस अध्याय में संसद, कार्यपालिका और न्यायपालिका की भूमिका और कार्यप्रणाली को सरल भाषा में समझाया गया है।
यह विद्यार्थियों को भारत के संसदीय ढांचे और सत्ता के विभाजन की गहरी समझ प्रदान करता है।
| पाठ्यपुस्तक | NCERT / SCERT |
| कक्षा | कक्षा 9 |
| विषय | राजनीति विज्ञान |
| अध्याय | अध्याय 5 |
| प्रकरण | संसदीय लोकतंत्र की संस्थाएँ |
Bihar Board Class 9 राजनीति विज्ञान अध्याय 5 संसदीय लोकतंत्र की संस्थाएँ के प्रश्नों का उत्तर:
1. अगर आप भारत का राष्ट्रपति चुना जाए तो अपने निम्नलिखित में से कौन सा फैसला खुद कर सकते हैं?
(क) अपनी पसंद के व्यक्ति को प्रधानमंत्री चुन सकते हैं।
(ख) लोकसभा में बहुमत वाले प्रधानमंत्री को उसके पद से हटा सकते हैं।
(ग) दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं।
(घ) मंत्रिपरिषद में अपनी पसंद के नेताओं का चयन कर सकते हैं।
उत्तर: (ग) दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं।
स्पष्टीकरण: राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित विधेयकों को पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, लेकिन अपनी पसंद से प्रधानमंत्री या मंत्रियों का चयन नहीं कर सकते।
2. निम्नलिखित में कौन राजनैतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है?
(क) जिलाधीश
(ख) गृह मंत्रालय का सचिव
(ग) गृह मंत्री
(घ) पुलिस महानिदेशक
उत्तर: (ग) गृह मंत्री
स्पष्टीकरण: गृह मंत्री एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि होते हैं और कैबिनेट में शामिल होते हैं। बाकी सभी प्रशासनिक पदाधिकारी होते हैं।
3. न्यायपालिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा बयान गलत है?
(क) संसद द्वारा पारित प्रत्येक कानून को सर्वोच्च न्यायालय की मंजूरी की जरूरत होती है।
(ख) अगर कोई कानून संविधान की भावना के खिलाफ है तो न्यायपालिका उसे अमान्य घोषित कर सकती है।
(ग) न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्रता होती है।
(घ) अगर किसी नागरिक के अधिकारों का हनन होता है तो वह अदालत में जा सकता है।
उत्तर: (क) संसद द्वारा पारित प्रत्येक कानून को सर्वोच्च न्यायालय की मंजूरी की जरूरत होती है।
स्पष्टीकरण: संसद द्वारा पारित कानून को सर्वोच्च न्यायालय की मंजूरी नहीं लेनी होती। न्यायालय केवल तब हस्तक्षेप करता है जब किसी कानून की संवैधानिकता पर सवाल उठे।
4. निम्नलिखित राजनीतिक संस्थानों में से कौन सी संस्था देश के मौजूदा कानून में संशोधन कर सकती है?
(क) सर्वोच्च न्यायालय
(ख) राष्ट्रपति
(ग) प्रधानमंत्री
(घ) सांसद
उत्तर: (घ) सांसद
स्पष्टीकरण: केवल संसद के सदस्य (MPs) ही संविधान और कानूनों में संशोधन कर सकते हैं।
5. उसे मंत्रालय की पहचान करें जिसने निम्नलिखित समाचार जारी किया होगा:
| (क) देश से जुट का निर्यात बढ़ाने के लिए एक नई नीति बनाई जा रही है। | (4) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय |
| (ख) ग्रामीण इलाकों में टेलीफोन सेवाएं सुलभ कराई जाएगी। | (1) दूरसंचार विभाग (लेकिन विकल्पों में सही नाम न होने पर — रक्षा मंत्रालय गलत है।) सही मंत्रालय: दूरसंचार मंत्रालय / संचार मंत्रालय होना चाहिए। (यदि यह विकल्प उपलब्ध हो) |
| (ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत बिकने वाले चावल और गेहूं की कीमतें कम की जाएगी। | (3) कृषि, खाद्यान्न और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय |
| (घ) पल्स पोलियो अभियान शुरू किया जाएगा। भत्ते बढ़ाए जाएंगे। | (2) स्वास्थ्य मंत्रालय |
6: देश की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में से उस राजनीतिक संस्था का नाम बताइए जो निम्नलिखित मामलों में अधिकारों का इस्तेमाल करती है —
(क) सड़क, सिंचाई जैसे बुनियादी ढांचों के विकास और नागरिकों की विभिन्न कल्याणकारी गतिविधियों पर कितना पैसा खर्च किया जाएगा।
उत्तर: कार्यपालिका (Executive)
(ख) स्टॉक एक्सचेंज को नियमित करने संबंधी कानून बनाने की कमेटी के सुझाव पर विचार-विमर्श करती है।
उत्तर: विधायिका (Legislature)
(ग) दो राज्य सरकारों के बीच कानूनी विवाद पर निर्णय लेती है।
उत्तर: न्यायपालिका (Judiciary)
(घ) भूकंप पीड़ितों की राहत के प्रयासों के बारे में सूचना मांगती है।
उत्तर: विधायिका (Legislature)
7. भारत का प्रधानमंत्री सीधे जनता द्वारा क्यों नहीं चुना जाता? निम्नलिखित चार जवाबों में सबसे सही को चुनकर अपनी पसंद के पक्ष में कारण दीजिए:
(क) संसदीय लोकतंत्र में लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी का नेता ही प्रधानमंत्री बन सकता है।
(ख) लोकसभा, प्रधानमंत्री और मंत्रीपरिषद का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही उन्हें हटा सकती है।
(ग) चूंकि प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति नियुक्त करता है लिहाजा उसे जनता द्वारा चुने जाने की जरूरत ही नहीं है।
(घ) प्रधानमंत्री के सीधे चुनाव में बहुत ज्यादा खर्च आएगा।
उत्तर: (क) संसदीय लोकतंत्र में लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी का नेता ही प्रधानमंत्री बन सकता है।
✅ कारण:
- भारत संसदीय लोकतंत्र (Parliamentary Democracy) को अपनाता है, जिसमें जनता प्रतिनिधियों को चुनती है, न कि सीधे प्रधानमंत्री को।
- जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि लोकसभा में बहुमत प्राप्त करते हैं, और वही बहुमत दल (या गठबंधन) अपने नेता को प्रधानमंत्री चुनता है।
- इस प्रणाली में प्रधानमंत्री को लोकसभा के प्रति जवाबदेह बनाया जाता है। यदि वह विश्वास खो देता है तो संसद उसे हटा सकती है।
- सीधे चुनाव की स्थिति में यह जवाबदेही कमजोर पड़ सकती है और संवैधानिक संतुलन बिगड़ सकता है।
📌 निष्कर्ष: भारत में प्रधानमंत्री का सीधा चुनाव न होना लोकतंत्र की मजबूती और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करता है।
8. तीन दोस्त एक ऐसी फिल्म देखने गए जिनमें हीरो एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनता है और राज्य में बहुत से बदलाव लाता है। इमरान ने कहा कि देश को ऐसी चीज की जरूरत है। रिजवान कहा कि इस तरह का बिना संस्थाओं वाला एक व्यक्ति का राज खतरनाक है। शंकर ने कहा कि यह तो एक कल्पना है। कोई भी मंत्री एक दिन में कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसी फिल्मों के बारे में आपकी क्या राय है?
उत्तर:
ऐसी फिल्मों का उद्देश्य आमतौर पर मनोरंजन होता है, लेकिन ये जनता को राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था पर सोचने के लिए प्रेरित भी कर सकती हैं।
- ✅ इमरान की बात में कुछ सच्चाई है कि देश को बदलाव की जरूरत है, लेकिन यह बदलाव व्यक्तिगत शासन से नहीं, बल्कि प्रणालियों में सुधार से आना चाहिए।
- ✅ रिज़वान सही कहते हैं कि बिना संस्थाओं के शासन तानाशाही की ओर ले जा सकता है। लोकतंत्र की सुंदरता इसमें है कि हर निर्णय संविधानिक संस्थाओं और प्रक्रियाओं के तहत होता है।
- ✅ शंकर की बात व्यावहारिक है — कोई मंत्री एक दिन में सब कुछ नहीं बदल सकता क्योंकि शासन एक समूहिक और संस्थागत प्रक्रिया है, जो समय लेती है।
📌 निष्कर्ष: ऐसी फिल्में प्रेरणादायक हो सकती हैं, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि लोकतंत्र में परिवर्तन संस्थागत प्रक्रिया और नागरिक भागीदारी के माध्यम से ही संभव है, न कि केवल एक व्यक्ति की शक्ति से।
9. एक शिक्षिका छात्रों की संसद के आयोजन की तैयारी कर रही थी। उसने दो छात्राओं से अलग-अलग पार्टियों के नेताओं की भूमिका करने को कहा। उसने उन्हें विकल्प भी दिया। यदि वे चाहें तो राज्यसभा में बहुमत प्राप्त दल की नेता हो सकती थी और अगर चाहे तो लोकसभा के बहुमत प्राप्त दल की। अगर आपको यह विकल्प दिया गया तो आप क्या चुनेंगे और क्यों?
उत्तर:
यदि मुझे यह विकल्प दिया जाए कि मैं राज्यसभा में बहुमत प्राप्त दल की नेता बनूं या लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल की, तो मैं लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल की नेता बनना पसंद करूंगा।
कारण इस प्रकार हैं:
- ✅ लोकसभा भारत की प्रमुख विधायी संस्था है, जहां से प्रधानमंत्री का चयन होता है। बहुमत प्राप्त दल की नेता होने का अर्थ है कि मैं प्रधानमंत्री बन सकता/सकती हूँ।
- ✅ लोकसभा सीधे जनता द्वारा चुनी जाती है, इसलिए इसकी लोकतांत्रिक वैधता अधिक होती है।
- ✅ लोकसभा के निर्णय देश की नीति निर्धारण में प्रभावशाली भूमिका निभाते हैं।
- ✅ बहुमत दल की नेता होने से मेरे पास सरकार बनाने और चलाने का अधिकार होता है, जो राज्यसभा की तुलना में अधिक शक्तिशाली भूमिका है।
📌 निष्कर्ष: लोकसभा में बहुमत दल की नेता बनना अधिक जिम्मेदारीपूर्ण और प्रभावशाली पद होता है, क्योंकि इसमें जनता की सीधी भागीदारी और नीति निर्माण में अग्रणी भूमिका होती है।
10. आरक्षण पर आदेश का उदाहरण पढ़कर तीन विद्यार्थियों की न्यायपालिका की भूमिका पर अलग-अलग प्रतिक्रिया थी। इनमें से कौन सी प्रतिक्रिया न्यायपालिका की भूमिका को सही तरह से समझती है?
(क) श्रीनिवास का तर्क है कि चूंकि सर्वोच्च न्यायालय सरकार के साथ सहमत हो गई है लिहाजा वह स्वतंत्र नहीं है।
(ख) अंजैया का कहना है कि न्यायपालिका स्वतंत्र है क्योंकि वह सरकार के आदेश के खिलाफ फैसला सुना सकती थी। सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को उसमें संशोधन का निर्देश दिया।
(ग) विजया का मानना है कि न्यायपालिका ना तो स्वतंत्र है ना ही किसी के अनुसार चलने वाली है बल्कि वह विरोधी समूहों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाती है। न्यायालय ने इस आदेश के समर्थकों और विरोधियों के बीच बढ़िया संतुलन बनाए।
आपकी राय में कौन सा विचार सबसे सही है?
उत्तर: (ग) विजया का विचार सबसे सही है।
तर्क:
विजया ने न्यायपालिका की भूमिका को सबसे संतुलित और गहराई से समझा है। उसने बताया कि—
- ✅ न्यायपालिका न तो पूरी तरह सरकार की पक्षधर होती है और न ही किसी विरोधी समूह की।
- ✅ उसका कार्य न्याय करना और संतुलन बनाना होता है, जिससे समाज के सभी वर्गों के हितों की रक्षा हो सके।
- ✅ अदालत ने आरक्षण पर निर्णय देते समय समर्थक और विरोधी दोनों पक्षों की बातों को ध्यान में रखते हुए फैसला सुनाया, जिससे वह निष्पक्ष बनी रही।
📌 निष्कर्ष: विजया का विचार सही है क्योंकि उसने यह समझा कि न्यायपालिका का कार्य पक्षपात करना नहीं, बल्कि संविधान और कानून के अनुसार न्यायपूर्ण एवं संतुलित निर्णय देना है। यह लोकतंत्र के लिए अनिवार्य है।
11. बिहार विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है?
उत्तर: बिहार विधानसभा में कुल 243 सदस्य होते हैं, जिन्हें जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है।
12. बिहार विधान परिषद का गठन कैसे होता है?
उत्तर: बिहार विधान परिषद एक स्थायी सदन है, जिसका गठन विभिन्न क्षेत्रों से चुने और नामित किए गए सदस्यों से होता है। इसके गठन की प्रक्रिया इस प्रकार है:
- 🔹 स्थानीय निकायों से चुने जाते हैं — 1/3 सदस्य
- 🔹 शिक्षकों द्वारा चुने जाते हैं — 1/12 सदस्य
- 🔹 स्नातकों द्वारा चुने जाते हैं — 1/12 सदस्य
- 🔹 विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं — 1/3 सदस्य
- 🔹 राज्यपाल द्वारा नामित किए जाते हैं — शेष सदस्य (जो साहित्य, विज्ञान, कला, सामाजिक सेवा आदि क्षेत्रों से हों)
👉 इस तरह बिहार विधान परिषद में कुल 75 सदस्य होते हैं।
📌अन्य महत्वपूर्ण पोस्ट:
Bihar Board Class 9 राजनीति विज्ञान अध्याय 4 चुनावी राजनीति
Bihar Board Class 9 राजनीति विज्ञान अध्याय 6. लोकतांत्रिक अधिकार
